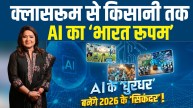Bharat Ek Soch: बिहार एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। लोग अपने वोट की ताकत से तय करेंगे कि कौन बिहार की सत्ता संभालेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा? लेकिन, इस बार बिहार के लोग किस आधार पर मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पर, बदलाव के मुद्दे पर, रोजगार के लिए पलायन रोकने के मुद्दे पर, बेहतर स्कूल-कॉलेज के मुद्दे पर, आर्थिक तरक्की के मुद्दे पर, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर, औद्योगिक विकास के मुद्दे पर या आखिर में जाति का जुगाड़ ही चलेगा? बिहार जातीय राजनीति की एक मुखर प्रयोगशाला रहा है। बिहार के सियासी अखाड़े में खड़े बड़े-बड़े नेता भले ही विकास और बदलाव की बातें कर रहे हों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें कर रहे हों, लेकिन भीतरखाने जातीय समीकरण साधने के लिए बहुत सावधानी से गोटियां चली जा रही हैं। ऐसे में जाति आधारित छोटे दलों की पूछ बढ़ गयी है। मुकेश सहनी की VIP हो या उपेंद्र कुशवाहा की RLM, जीतनराम माझी की HAM हो या चिराग पासवान की LJP-R जैसी पार्टियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला चुन रखा है। बड़े राजनीतिक दलों की मजबूरी ये है कि जाति आधारित छोटे दलों से साथ आने से उनकी ताकत बढ़ जाती है, तो उनके विरोध से अधिक नुकसान के ग्रह-गोचर बनने लगते हैं। बिहार की चुनावी राजनीति में अगड़ा-पिछड़ा आजादी के पहले से ही शुरू हो चुका था। आजादी के शुरुआती 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता में सवर्णों का वर्चस्व रहा। उसके बाद पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी दिलाने की राजनीति शुरू हुई, लेकिन 1960 के दशक में बिहार में पिछड़ों की आवाज बुलंद करने वाले ज्यादातर नेता सवर्ण जाति से ताल्कुल रखते थे। यही वजह है कि 1967 में बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के मुखिया भी कायस्थ जाति के महामाया प्रसाद सिन्हा बने। जाति के करंट से सत्ता के लिए उमंग तैयार करने का काम तूफानी रफ्तार से चला। डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की सोशलिस्ट धारा और जेपी आंदोलन से निकले कुछ युवा नेताओं ने बिहार में जाति की राजनीति को नया आकार दिया। इसमें लालू प्रसाद यादव भी है, नीतीश कुमार भी, अब इस दुनिया में नहीं रहे रामविलास पासवान और शरद यादव भी। 1990 के दशक की शुरुआत में लालू यादव ने मुस्लिम प्लस यादव समीकरण के आधार पर बिहार में 15 साल राज किया। यादवों का वर्चस्व बढ़ा तो उसके विरोध में दूसरी पिछड़ी जातियां लामबंद हुईं। साल 2005 में नीतीश कुमार ने नए जातीय समीकरणों को साधते हुए सत्ता हासिल की। बिहार के नेताओं ने विकास और बदलाव की जगह जातीय समीकरणों पर अधिक माथापच्ची की। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने की किस तरह से जुगत चल रही है। पिछले 35 साल यानी लालू-नीतीश के दौर में बिहार में जाति की दीवार कितनी ऊंची हुई? बिहार में बीजेपी किस तरह जातीय गोलबंदी की स्क्रिप्ट पर काम करती रही है? बिहार में कैसे टूटा अगड़ी जातियों का राजनीति वर्चस्व और पिछड़ों को अगड़ा बनाने की राजनीति अब किस ओर बढ़ रही है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे।
सत्ता के लिए वोटों की सोशल इंजीनियरिंग
जाति जड़ नहीं जीवंत है। हमारे सामाजिक ताने-बाने की सच्चाई है। सामाजिक रिश्तों का आधार और पहचान है, लेकिन हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव जीतने के लिए जातियों के जोड़-तोड़ का प्रयोग जारी है। इससे समाज में जाति की दीवार गिरने की जगह और ऊंची होती जा रही है। भीतरखाने जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता हासिल करने के लिए समीकरण बैठाने की होड़ में शायद ही कोई राजनीतिक दल पीछे हो। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कलवार जाति से आते हैं। उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से हैं। उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की जाति भूमिहार है। जेडीयू के सबसे बड़े चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की, चिराग पासवान की पार्टी हो या मुकेश सहनी की, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। आरजेडी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर धानुक जाति से ताल्लुक रखने वाले मंगनी लाल मंडल को बैठाया है, तो कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी। मकसद साफ है-सत्ता के लिए वोटों की सोशल इंजीनियरिंग। ऐसे में अधिक सीटें जीतने के लिए सियासी दलों में कास्ट कॉम्बिनेशन पर लगातार जोड़ घटाव चल रहा है।
यह भी पढ़ें: क्या भरोसे के लायक बचा है चीन, भारत के पास क्या हैं रास्ते?
नीतीश की राजनीति का कैसे हुआ उदय?
बिहार में इन दिनों लोगों के बीच बातचीत का सबसे हॉट टॉपिक है कि अबकी बार किस जाति का वोट किसके पक्ष में जाएगा? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के साथ कौन-कौन सी जातियों का वोट जुड़ेगा? लालू यादव ने कभी MY यानि मुस्लिम+यादव वोट बैंक का कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसे विस्तार देते हुए तेजस्वी यादव महिला+यूथ कॉम्बिनेशन की बात कहते हैं। दो साल पहले आईं बिहार सरकार की जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि सूबे में यादव सबसे बड़ी जाति है। सूबे की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 14% से अधिक है। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में ओबीसी की हिस्सेदारी 63.14% है । जिसमें दो कैटगरी है एक Backward Classes और दूसरी Extremely Backward Classes. ऐसे में बिहार में ओबीसी वोटबैंक को अपनी ओर खींचने के लिए तरंग पैदा करने की कोशिश हो रही है। 1990 के दशक में लालू यादव ने यादव प्लस मुस्लिम वोटबैंक को साधते हुए सत्ता समीकरण बनाया, जिसमें यादव मजबूत हुए। मुस्लिमों में भी कुछ जातियों को ही सत्ता का फायदा मिला। लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की आंधी में सूबे की अगड़ी जातियां किनारे लग गईं। उनके दौर में यादवों का समाज से सत्ता प्रतिष्ठान तक प्रभाव बढ़ा। इससे माइनस यादव ओबीसी जातियों में नाराजगी बढ़ने लगी। इसी जातीय असंतोष से कुर्मी राजनीति का उदय हुआ, जिसके चेहरा बने नीतीश कुमार। साल 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने जातीय समीकरणों को साधने के साथ विकास का इंजन भी जोड़ दिया। उन्होंने लालू-राबड़ी राज में यादवों की तुलना में पिछड़ी ओबीसी जातियों के साथ दलितों में महादलित और मुस्लिमों में पसमंदा को अपने साथ जोड़ा। नीतीश कुमार की मॉडरेट सोशलिस्ट छवि की वजह से उन्हें अगड़ी जातियों का भी साथ मिलने लगा।
अगड़ा-पिछड़ा की लड़ाई में इस वर्ग का हुआ नुकसान
बिहार की राजनीति लालू यादव और नीतीश की परिक्रमा करने लगी। चुनावों में एक खास तरह का पैटर्न देखा जाने लगा। लोग किसी खास उम्मीदवार या दल चुनाव में जीताने की जगह दूसरे को सत्ता में आने से रोकने के लिए वोटिंग करने लगे। अगड़ा-पिछड़ा की लड़ाई में बिहार का सबसे अधिक नुकसान ये हुआ कि सूबे का पढ़ा-लिखा वर्ग तेजी से बाहर निकलने लगा। ब्यूरोक्रेसी में ज्यादातर अफसर ऊंची जातियों के थे, जिन्हें सामाजिक न्याय की राजनीति के झंडाबरदार अहम पदों पर बैठाना नहीं चाहते थे। नतीजा ये रहा कि कुछ Deputation पर बाहर निकल गए, तो कुछ बिहार में ही अपनी तैनाती के हिसाब से हालात बदलने का इंतजार करते रहे। ये भी बिहार की राजनीतिक चरित्रदोष और सत्ता की प्यास है कि जिस गैर कांग्रेसवाद की धारा से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का राजनीतिक उदय हुआ। वहीं लालू यादव कांग्रेस की मदद से बिहार में सरकार बनाते हैं। वहीं, नीतीश कुमार कांग्रेस की मदद से अपनी सरकार बचाते हैं। ये भी बिहार की राजनीति में जातियों का प्रभाव और कालचक्र है, जिसमें कभी अगड़ी जातियों के नेताओं के पीछे पिछड़ी जातियों के नेता खड़ा हुआ करते थे। आज की तारीख में पिछड़ी जातियों के नेताओं के पीछे अगड़ी जातियों के नेता अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार की सत्ता में पिछड़ी जातियों के सत्ता के केंद्र बिंदु में आने की कहानी समझने की लिए साल 1967 पर जाना होगा। जब नारा लगता था-संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में साठ। दरअसल, 1960 के दशक में सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया ने बिहार और यूपी में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी शुरू की, जिसका साइड इफेक्ट ये रहा कि आजादी के 20 साल के भीतर ही बिहार में सत्ता सवर्णों के हाथ से निकल कर पिछड़ा समुदाय के हाथों में चली गई।
बंगाल वाला बिहार कैसा था?
समाज और सत्ता का चक्र हमेशा घूमता रहता है। कभी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई थी। अब पिछड़ों में अगड़ा-पिछड़ा की चल रही है। आजादी के बाद के शुरुआती 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता में सवर्णों का वर्चस्व रहा। इसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जातियों के लोग शामिल थे। दरअसल, साल 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार के अलग राज्य बनने को जाति और राजनीतिक समन्वय की सफलता के बड़े केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है। जब बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, तब बंगाली सवर्ण सबसे ज्यादा अंग्रेजी के जानकार थे। बाद में कायस्थ और मुस्लिमों ने अंग्रेजी शिक्षा में खासी दिलचस्पी दिखाई। कायस्थों ने सरकारी दफ्तरों में बंगाली वर्चस्व को चुनौती देते हुए बड़ा आंदोलन खड़ा किया और अलग बिहार राज्य की मांग की। उस दौर में कायस्थों का नारा हुआ करता था-बिहार बिहारियों के लिए। जब साल 1912 में बिहार अलग राज्य बना तो हर क्षेत्र में नए-नए अवसर पैदा हुए, जिसका फायदा खासतौर से अंग्रेजी पढ़े लिए कायस्थों और मुस्लिमों के एक छोटे से वर्ग ने उठाया। बिहार में कायस्थ जाति के वर्चस्व को चुनौती मिली भूमिहार जाति से। बाद में भूमिहारों को चुनौती देने के लिए कायस्थ और राजपूतों ने हाथ मिलाया। जाति के आधार पर सियासी समीकरण बैठाने की परंपरा का श्रीगणेश हो चुका था। साल 1946 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने 76 सीटों में 18 पर राजपूत, 15 भूमिहार ब्राह्मण और 13 कायस्थों को टिकट दिया…वहीं पिछड़ी जातियों के 8 सदस्यों को टिकट मिला। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में भी जाति के मुद्दे पर जमकर तनतनी और गुटबाजी हुई, तब भूमिहारों के बड़े नेता श्रीकृष्ण सिंह थे। इस गुट ने कायस्थों के बड़े नेता कृष्णवल्लभ सहाय को अपनी ओर मिला लिया। राजपूत समुदाय के बड़े नेता अनुग्रह नारायण सिंह को भी साथ जोड़ लिया गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे श्रीकृष्ण सिंह और जयप्रकाश नारायण ने इसे भूमिहार राज का नाम दिया।
अब तक बिहार की राजनीति में किस जाति की कितनी हिस्सेदारी
सत्ता में हिस्सेदारी किसी भी जाति या समुदाय की ताकत कैसे बढ़ती और घटती है। इसे एक आंकड़े के जरिए समझा जा सकता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी में साल 1934 में कायस्थों की भागीदारी 53.84% थीं, तो राजपूत समुदाय के लोगों की 7.70% और भूमिहारों की 15.38%, लेकिन साल 1952 में कायस्थों की भागीदारी घटकर 5.26% पर आग गई। राजपूतों की हिस्सेदारी बढ़कर 26.33% हो गयी। भूमिहारों की 21.05%। इस दौरान ब्राह्मणों ने भी बिहार के राजनीतिक आसमान में अपनी जगह मजबूत की। साल 1957 में बिहार विधानसभा 210 सदस्यों में से जाति के आधार पर हिस्सेदारी को देखा जाए तो भूमिहार जाति के 34, राजपूत जाति के 30, ब्राह्मण समुदाय से 20 और कायस्थ जाति से 8 सदस्य विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं, साल 2020 में बिहार में 28 राजपूत, 21 भूमिहार, 21 ब्राह्मण और 3 कायस्थ जाति के उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। कभी जिस बिहार में भूमिहारों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता था। नए सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सवर्णों में सबसे बुरी स्थिति इसी जाति के लोगों की है। साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो उस साल यादव जाति के 63 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। अगले चुनाव यानी 1995 में ये संख्या बढ़कर 86 तक पहुंच गयी। लेकिन, 2020 के बिहार चुनाव में यादव विधायकों की संख्या 54 पर आ गईं, जिसमें से लालटेन चुनाव चिन्ह से सिर्फ 36 यादव ही विधायक बने। बिहार का इतिहास गवाह है कि जातियों से सत्ता को ताकत मिली और सत्ता से जातियों के भीतर खास लोगों को। सत्ता के लिए जातीय समीकरण साधने में बिहार के तरक्की की रफ्तार सुस्त होती गई। उस जकड़न से समाज को और सियासत को आजादी नहीं मिल पायीं, जिसके केंद्र में सबका साथ और सबका विकास का एजेंडा हो।
यह भी पढ़ें: दर्द-ए-बिहार: क्या बिहार में अपराधियों को कानून और पुलिस का डर नहीं रहा, क्यों बढ़ रहा क्राइम?
Bharat Ek Soch: बिहार एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। लोग अपने वोट की ताकत से तय करेंगे कि कौन बिहार की सत्ता संभालेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा? लेकिन, इस बार बिहार के लोग किस आधार पर मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पर, बदलाव के मुद्दे पर, रोजगार के लिए पलायन रोकने के मुद्दे पर, बेहतर स्कूल-कॉलेज के मुद्दे पर, आर्थिक तरक्की के मुद्दे पर, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर, औद्योगिक विकास के मुद्दे पर या आखिर में जाति का जुगाड़ ही चलेगा? बिहार जातीय राजनीति की एक मुखर प्रयोगशाला रहा है। बिहार के सियासी अखाड़े में खड़े बड़े-बड़े नेता भले ही विकास और बदलाव की बातें कर रहे हों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें कर रहे हों, लेकिन भीतरखाने जातीय समीकरण साधने के लिए बहुत सावधानी से गोटियां चली जा रही हैं। ऐसे में जाति आधारित छोटे दलों की पूछ बढ़ गयी है। मुकेश सहनी की VIP हो या उपेंद्र कुशवाहा की RLM, जीतनराम माझी की HAM हो या चिराग पासवान की LJP-R जैसी पार्टियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला चुन रखा है। बड़े राजनीतिक दलों की मजबूरी ये है कि जाति आधारित छोटे दलों से साथ आने से उनकी ताकत बढ़ जाती है, तो उनके विरोध से अधिक नुकसान के ग्रह-गोचर बनने लगते हैं। बिहार की चुनावी राजनीति में अगड़ा-पिछड़ा आजादी के पहले से ही शुरू हो चुका था। आजादी के शुरुआती 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता में सवर्णों का वर्चस्व रहा। उसके बाद पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी दिलाने की राजनीति शुरू हुई, लेकिन 1960 के दशक में बिहार में पिछड़ों की आवाज बुलंद करने वाले ज्यादातर नेता सवर्ण जाति से ताल्कुल रखते थे। यही वजह है कि 1967 में बिहार की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के मुखिया भी कायस्थ जाति के महामाया प्रसाद सिन्हा बने। जाति के करंट से सत्ता के लिए उमंग तैयार करने का काम तूफानी रफ्तार से चला। डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की सोशलिस्ट धारा और जेपी आंदोलन से निकले कुछ युवा नेताओं ने बिहार में जाति की राजनीति को नया आकार दिया। इसमें लालू प्रसाद यादव भी है, नीतीश कुमार भी, अब इस दुनिया में नहीं रहे रामविलास पासवान और शरद यादव भी। 1990 के दशक की शुरुआत में लालू यादव ने मुस्लिम प्लस यादव समीकरण के आधार पर बिहार में 15 साल राज किया। यादवों का वर्चस्व बढ़ा तो उसके विरोध में दूसरी पिछड़ी जातियां लामबंद हुईं। साल 2005 में नीतीश कुमार ने नए जातीय समीकरणों को साधते हुए सत्ता हासिल की। बिहार के नेताओं ने विकास और बदलाव की जगह जातीय समीकरणों पर अधिक माथापच्ची की। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने की किस तरह से जुगत चल रही है। पिछले 35 साल यानी लालू-नीतीश के दौर में बिहार में जाति की दीवार कितनी ऊंची हुई? बिहार में बीजेपी किस तरह जातीय गोलबंदी की स्क्रिप्ट पर काम करती रही है? बिहार में कैसे टूटा अगड़ी जातियों का राजनीति वर्चस्व और पिछड़ों को अगड़ा बनाने की राजनीति अब किस ओर बढ़ रही है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे।
सत्ता के लिए वोटों की सोशल इंजीनियरिंग
जाति जड़ नहीं जीवंत है। हमारे सामाजिक ताने-बाने की सच्चाई है। सामाजिक रिश्तों का आधार और पहचान है, लेकिन हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव जीतने के लिए जातियों के जोड़-तोड़ का प्रयोग जारी है। इससे समाज में जाति की दीवार गिरने की जगह और ऊंची होती जा रही है। भीतरखाने जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता हासिल करने के लिए समीकरण बैठाने की होड़ में शायद ही कोई राजनीतिक दल पीछे हो। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कलवार जाति से आते हैं। उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से हैं। उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की जाति भूमिहार है। जेडीयू के सबसे बड़े चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की, चिराग पासवान की पार्टी हो या मुकेश सहनी की, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। आरजेडी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर धानुक जाति से ताल्लुक रखने वाले मंगनी लाल मंडल को बैठाया है, तो कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी। मकसद साफ है-सत्ता के लिए वोटों की सोशल इंजीनियरिंग। ऐसे में अधिक सीटें जीतने के लिए सियासी दलों में कास्ट कॉम्बिनेशन पर लगातार जोड़ घटाव चल रहा है।
यह भी पढ़ें: क्या भरोसे के लायक बचा है चीन, भारत के पास क्या हैं रास्ते?
नीतीश की राजनीति का कैसे हुआ उदय?
बिहार में इन दिनों लोगों के बीच बातचीत का सबसे हॉट टॉपिक है कि अबकी बार किस जाति का वोट किसके पक्ष में जाएगा? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के साथ कौन-कौन सी जातियों का वोट जुड़ेगा? लालू यादव ने कभी MY यानि मुस्लिम+यादव वोट बैंक का कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसे विस्तार देते हुए तेजस्वी यादव महिला+यूथ कॉम्बिनेशन की बात कहते हैं। दो साल पहले आईं बिहार सरकार की जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि सूबे में यादव सबसे बड़ी जाति है। सूबे की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 14% से अधिक है। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में ओबीसी की हिस्सेदारी 63.14% है । जिसमें दो कैटगरी है एक Backward Classes और दूसरी Extremely Backward Classes. ऐसे में बिहार में ओबीसी वोटबैंक को अपनी ओर खींचने के लिए तरंग पैदा करने की कोशिश हो रही है। 1990 के दशक में लालू यादव ने यादव प्लस मुस्लिम वोटबैंक को साधते हुए सत्ता समीकरण बनाया, जिसमें यादव मजबूत हुए। मुस्लिमों में भी कुछ जातियों को ही सत्ता का फायदा मिला। लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की आंधी में सूबे की अगड़ी जातियां किनारे लग गईं। उनके दौर में यादवों का समाज से सत्ता प्रतिष्ठान तक प्रभाव बढ़ा। इससे माइनस यादव ओबीसी जातियों में नाराजगी बढ़ने लगी। इसी जातीय असंतोष से कुर्मी राजनीति का उदय हुआ, जिसके चेहरा बने नीतीश कुमार। साल 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने जातीय समीकरणों को साधने के साथ विकास का इंजन भी जोड़ दिया। उन्होंने लालू-राबड़ी राज में यादवों की तुलना में पिछड़ी ओबीसी जातियों के साथ दलितों में महादलित और मुस्लिमों में पसमंदा को अपने साथ जोड़ा। नीतीश कुमार की मॉडरेट सोशलिस्ट छवि की वजह से उन्हें अगड़ी जातियों का भी साथ मिलने लगा।
अगड़ा-पिछड़ा की लड़ाई में इस वर्ग का हुआ नुकसान
बिहार की राजनीति लालू यादव और नीतीश की परिक्रमा करने लगी। चुनावों में एक खास तरह का पैटर्न देखा जाने लगा। लोग किसी खास उम्मीदवार या दल चुनाव में जीताने की जगह दूसरे को सत्ता में आने से रोकने के लिए वोटिंग करने लगे। अगड़ा-पिछड़ा की लड़ाई में बिहार का सबसे अधिक नुकसान ये हुआ कि सूबे का पढ़ा-लिखा वर्ग तेजी से बाहर निकलने लगा। ब्यूरोक्रेसी में ज्यादातर अफसर ऊंची जातियों के थे, जिन्हें सामाजिक न्याय की राजनीति के झंडाबरदार अहम पदों पर बैठाना नहीं चाहते थे। नतीजा ये रहा कि कुछ Deputation पर बाहर निकल गए, तो कुछ बिहार में ही अपनी तैनाती के हिसाब से हालात बदलने का इंतजार करते रहे। ये भी बिहार की राजनीतिक चरित्रदोष और सत्ता की प्यास है कि जिस गैर कांग्रेसवाद की धारा से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का राजनीतिक उदय हुआ। वहीं लालू यादव कांग्रेस की मदद से बिहार में सरकार बनाते हैं। वहीं, नीतीश कुमार कांग्रेस की मदद से अपनी सरकार बचाते हैं। ये भी बिहार की राजनीति में जातियों का प्रभाव और कालचक्र है, जिसमें कभी अगड़ी जातियों के नेताओं के पीछे पिछड़ी जातियों के नेता खड़ा हुआ करते थे। आज की तारीख में पिछड़ी जातियों के नेताओं के पीछे अगड़ी जातियों के नेता अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार की सत्ता में पिछड़ी जातियों के सत्ता के केंद्र बिंदु में आने की कहानी समझने की लिए साल 1967 पर जाना होगा। जब नारा लगता था-संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में साठ। दरअसल, 1960 के दशक में सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया ने बिहार और यूपी में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी शुरू की, जिसका साइड इफेक्ट ये रहा कि आजादी के 20 साल के भीतर ही बिहार में सत्ता सवर्णों के हाथ से निकल कर पिछड़ा समुदाय के हाथों में चली गई।
बंगाल वाला बिहार कैसा था?
समाज और सत्ता का चक्र हमेशा घूमता रहता है। कभी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई थी। अब पिछड़ों में अगड़ा-पिछड़ा की चल रही है। आजादी के बाद के शुरुआती 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता में सवर्णों का वर्चस्व रहा। इसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जातियों के लोग शामिल थे। दरअसल, साल 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार के अलग राज्य बनने को जाति और राजनीतिक समन्वय की सफलता के बड़े केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है। जब बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, तब बंगाली सवर्ण सबसे ज्यादा अंग्रेजी के जानकार थे। बाद में कायस्थ और मुस्लिमों ने अंग्रेजी शिक्षा में खासी दिलचस्पी दिखाई। कायस्थों ने सरकारी दफ्तरों में बंगाली वर्चस्व को चुनौती देते हुए बड़ा आंदोलन खड़ा किया और अलग बिहार राज्य की मांग की। उस दौर में कायस्थों का नारा हुआ करता था-बिहार बिहारियों के लिए। जब साल 1912 में बिहार अलग राज्य बना तो हर क्षेत्र में नए-नए अवसर पैदा हुए, जिसका फायदा खासतौर से अंग्रेजी पढ़े लिए कायस्थों और मुस्लिमों के एक छोटे से वर्ग ने उठाया। बिहार में कायस्थ जाति के वर्चस्व को चुनौती मिली भूमिहार जाति से। बाद में भूमिहारों को चुनौती देने के लिए कायस्थ और राजपूतों ने हाथ मिलाया। जाति के आधार पर सियासी समीकरण बैठाने की परंपरा का श्रीगणेश हो चुका था। साल 1946 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने 76 सीटों में 18 पर राजपूत, 15 भूमिहार ब्राह्मण और 13 कायस्थों को टिकट दिया…वहीं पिछड़ी जातियों के 8 सदस्यों को टिकट मिला। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में भी जाति के मुद्दे पर जमकर तनतनी और गुटबाजी हुई, तब भूमिहारों के बड़े नेता श्रीकृष्ण सिंह थे। इस गुट ने कायस्थों के बड़े नेता कृष्णवल्लभ सहाय को अपनी ओर मिला लिया। राजपूत समुदाय के बड़े नेता अनुग्रह नारायण सिंह को भी साथ जोड़ लिया गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे श्रीकृष्ण सिंह और जयप्रकाश नारायण ने इसे भूमिहार राज का नाम दिया।
अब तक बिहार की राजनीति में किस जाति की कितनी हिस्सेदारी
सत्ता में हिस्सेदारी किसी भी जाति या समुदाय की ताकत कैसे बढ़ती और घटती है। इसे एक आंकड़े के जरिए समझा जा सकता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी में साल 1934 में कायस्थों की भागीदारी 53.84% थीं, तो राजपूत समुदाय के लोगों की 7.70% और भूमिहारों की 15.38%, लेकिन साल 1952 में कायस्थों की भागीदारी घटकर 5.26% पर आग गई। राजपूतों की हिस्सेदारी बढ़कर 26.33% हो गयी। भूमिहारों की 21.05%। इस दौरान ब्राह्मणों ने भी बिहार के राजनीतिक आसमान में अपनी जगह मजबूत की। साल 1957 में बिहार विधानसभा 210 सदस्यों में से जाति के आधार पर हिस्सेदारी को देखा जाए तो भूमिहार जाति के 34, राजपूत जाति के 30, ब्राह्मण समुदाय से 20 और कायस्थ जाति से 8 सदस्य विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं, साल 2020 में बिहार में 28 राजपूत, 21 भूमिहार, 21 ब्राह्मण और 3 कायस्थ जाति के उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। कभी जिस बिहार में भूमिहारों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता था। नए सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सवर्णों में सबसे बुरी स्थिति इसी जाति के लोगों की है। साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो उस साल यादव जाति के 63 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। अगले चुनाव यानी 1995 में ये संख्या बढ़कर 86 तक पहुंच गयी। लेकिन, 2020 के बिहार चुनाव में यादव विधायकों की संख्या 54 पर आ गईं, जिसमें से लालटेन चुनाव चिन्ह से सिर्फ 36 यादव ही विधायक बने। बिहार का इतिहास गवाह है कि जातियों से सत्ता को ताकत मिली और सत्ता से जातियों के भीतर खास लोगों को। सत्ता के लिए जातीय समीकरण साधने में बिहार के तरक्की की रफ्तार सुस्त होती गई। उस जकड़न से समाज को और सियासत को आजादी नहीं मिल पायीं, जिसके केंद्र में सबका साथ और सबका विकास का एजेंडा हो।
यह भी पढ़ें: दर्द-ए-बिहार: क्या बिहार में अपराधियों को कानून और पुलिस का डर नहीं रहा, क्यों बढ़ रहा क्राइम?